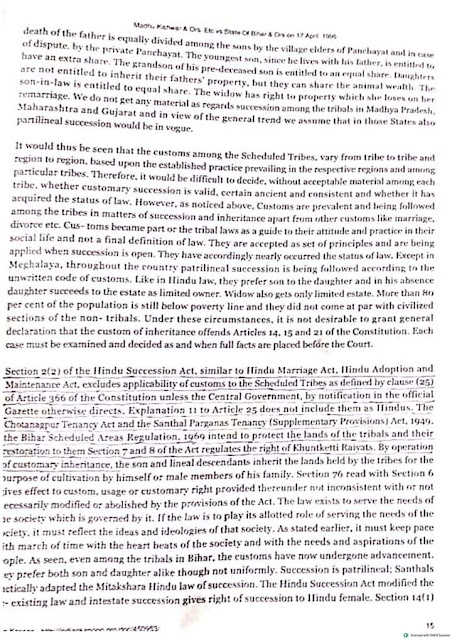आदिवासी हिंदू नहीं- क्योंकि तुलसी टिगे
विभिन्न न्यायालय के निर्णय, भारतीय संविधान, आदिवासी संस्कृति, बोली भाषा, देवी-देवता संबंधी मान्यता पूजा पद्धति, परंपरा, रीति-रिवाज, पुरातत्वीय शोध, मानव वंश, शास्त्र, शरीर रचना, विज्ञान, नस्ल-वंश, डीएनए रिसर्च इतिहास इत्यादि सभी तरह से सिद्ध हुआ है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। Adivasi Hindu Nahi |
न्यायालयीन निर्णय
- 1. माननीय सुप्रीम कोर्ट केस नं. 10367 ओर 2010 (5) जनवरी 2011) (भील)
- 2. माननीय हाईकोर्ट जबलपुर (मध्यप्रदेश) रेवन्यू निर्णय 100/1990 राम गुलाम बनाम नारायण (बहेलिया)
- 3. मध्यप्रदेश रेवन्यू निर्णय क्र. 191/1980 रामवती बनाम सहोदरी बाई (हल्या)
- 4. माननीय कुटुंब न्यायालय, बालोद (छ.ग.) बनिहारीन कराने भोयर (हल्या) प्रकरण क्र. 3/07 बाई बनाम जओहरू राम दिनांक 6-10-2009
- 5. सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत आदिवासी हल्या समाज चालोद महासभा से प्राप्त दस्तावेज सु. आ./09/64 दिनांक 15 सितंबर 2009
- 6. मध्यप्रदेश लो जनरल प्रकरण क्र. 21/1971-त्रिलोक सिंह विरूद्ध गुलबसिया बाई (गोंड)
- 7. आदिवासी कमेटी के सदस्य के रूप में जगाजल सिंह मुण्डा का संविधान सभा में भाषण (संविधान सभा चर्चाएँ ऑफिसियल रिपोर्ट खंड-१, खंड 11)
प्रकाशक-लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली 199
हिंदू धर्म के चारो वर्ण-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में से आदिवासी किसी भी वर्ण में नहीं आते। हम आदिवासियों को कोई भी प्रथा परंपरा, मान्यता एवं देवी-देवताओं का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों में कहीं नहीं है। इसलिए आदिवासी हिंदू नहीं है।आदिवासी हिंदू नहीं तो फिर क्या हैं? Adivasi Hindu Nahi
- जिस तरह पानी-जल-वाटर-समनार्थी हैं।
- जैसे क्रिश्चियन धर्म-ईसाई धर्म समनार्थी है।
- जैसे मुस्लिम धर्म-इस्लाम धर्म समानार्थी है।
- जैसे आर्य धर्म-वैदिक धर्म-हिंदू धर्म समानार्थी है।
- 1901 की जनगणना में अंग्रेजों ने प्रकृति वादी लिखा था।
- 1911 की जनगणना में अंग्रेजों ने जनजातिय धर्म/प्रकृति पूजक लिखा।
- 1931 की जनगणना में आदिम धर्म लिखा गया था।
हमें जो भी संवैधानिक अधिकार मिला है वो हिंदू होने से नहीं बल्कि आदिवासी होने से मिला है। हिंदू होने में आज तक एक भी फायदा नहीं हुआ और भविष्य में भी नहीं होगा। जय आदिवासी जागो आदिवासी आदिवासी भाइयों से निवेदन है कि इस विषय को वॉटसअप में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर अपना स्वयं को आदिवासी होने का सबूत देखें। कांकेर मो.: 9479158445
आदिवासी हिन्दू नहीं है। Adivasi Hindu Nahi सुप्रीम कोर्ट निर्णय मधु किश्वर अन्य बनाम बिहार राज्य 1996
इन दोनों रिट याचिकाओं में कानून का एक समान प्रश्न उठाया गया है: क्या महिला आदिवासी, बिना वसीयत के उत्तराधिकार में पुरुष आदिवासी के साथ समानता की हकदार हैं? पहली याचिकाकर्ता 'मानुषी' नामक पत्रिका की संपादक हैं, जो भारतीय महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने और उन्हें समान अधिकार दिलाने के लिए काम करती हैं।याचिकाकर्ता क्रमांक 2 श्रीमती सोनामुनी और 3 श्रीमती मुकी दुई क्रमशः मुकी बांगुमा की विधवा और विवाहित पुत्री हैं। वे बिहार राज्य के सिंहभूम जिले के सोनुआ प्रखंड के लोंगो गांव की हो जनजाति से हैं। रिट याचिका क्रमांक 219/86 में याचिकाकर्ता जुलियाना लकड़ा छोटा नागपुर क्षेत्र की एक उरांव ईसाई आदिवासी महिला हैं।
वे यह घोषित करने की मांग कर रही हैं कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 6/1908 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धाराएं 7, 8 और 76, उनका तर्क है कि बिहार राज्य और देश के अन्य भागों में प्रचलित प्रथागत कानून आदिवासी महिलाओं को भूमि या संपत्ति के उत्तराधिकार से वंचित करता है।
पिता की मृत्यु के पश्चात् गांव के बुजुर्गों द्वारा तथा विवाद की स्थिति में निजी पंचायत द्वारा संपत्ति को बेटों में बराबर-बराबर बांटा जाता है। चूंकि सबसे छोटा बेटा अपने पिता के साथ रहता है, इसलिए उसे अतिरिक्त हिस्सा मिलता है। मृतक बेटे के पोते को बराबर हिस्सा मिलता है।
पिता की मृत्यु के पश्चात् गांव के बुजुर्गों द्वारा तथा विवाद की स्थिति में निजी पंचायत द्वारा संपत्ति को बेटों में बराबर-बराबर बांटा जाता है। चूंकि सबसे छोटा बेटा अपने पिता के साथ रहता है, इसलिए उसे अतिरिक्त हिस्सा मिलता है। मृतक बेटे के पोते को बराबर हिस्सा मिलता है।
बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता, लेकिन वे पशु धन में हिस्सा ले सकती हैं। दामाद को बराबर हिस्सा मिलता है। विधवा को संपत्ति में अधिकार होता है, जिसे वह दोबारा शादी करने पर खो देती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में आदिवासियों के बीच उत्तराधिकार के संबंध में हमें कोई सामग्री नहीं मिलती है और सामान्य प्रवृत्ति को देखते हुए हम यह मान लेते हैं कि उन राज्यों में भी पक्षपातपूर्ण उत्तराधिकार प्रचलित होगा।
इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि अनुसूचित जनजातियों के बीच रीति-रिवाज, जनजाति से जनजाति और क्षेत्र से क्षेत्र में भिन्न-भिन्न होते हैं, जो संबंधित क्षेत्रों और विशेष जनजातियों में प्रचलित स्थापित प्रथा पर आधारित होते हैं। इसलिए, प्रत्येक जनजाति के बीच स्वीकार्य सामग्री के बिना यह तय करना कठिन होगा कि क्या प्रथागत उत्तराधिकार वैध है, निश्चित प्राचीन और सुसंगत है और क्या इसने कानून का दर्जा प्राप्त कर लिया है।
इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि अनुसूचित जनजातियों के बीच रीति-रिवाज, जनजाति से जनजाति और क्षेत्र से क्षेत्र में भिन्न-भिन्न होते हैं, जो संबंधित क्षेत्रों और विशेष जनजातियों में प्रचलित स्थापित प्रथा पर आधारित होते हैं। इसलिए, प्रत्येक जनजाति के बीच स्वीकार्य सामग्री के बिना यह तय करना कठिन होगा कि क्या प्रथागत उत्तराधिकार वैध है, निश्चित प्राचीन और सुसंगत है और क्या इसने कानून का दर्जा प्राप्त कर लिया है।
हालाँकि, जैसा कि ऊपर देखा गया है, विवाह, तलाक आदि अन्य प्रथाओं के अलावा उत्तराधिकार और विरासत के मामलों में जनजातियों के बीच रीति-रिवाज प्रचलित हैं और उनका पालन किया जा रहा है। रीति-रिवाज आदिवासी कानूनों का हिस्सा बन गए हैं, जो उनके सामाजिक जीवन में उनके दृष्टिकोण और व्यवहार के मार्गदर्शक हैं, न कि कानून की अंतिम परिभाषा।
उन्हें सिद्धांतों के एक समूह के रूप में स्वीकार किया जाता है और उत्तराधिकार खुला होने पर लागू किया जाता है। तदनुसार उन्होंने लगभग कानून का दर्जा प्राप्त कर लिया है। मेघालय को छोड़कर, पूरे देश में पितृवंशीय उत्तराधिकार का पालन अलिखित रीति-रिवाजों के अनुसार किया जा रहा है।
हिंदू कानून की तरह, वे बेटी की तुलना में बेटे को प्राथमिकता देते हैं इन परिस्थितियों में, यह सामान्य घोषणा करना वांछनीय नहीं है कि उत्तराधिकार की प्रथा संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करती है। प्रत्येक मामले की जांच की जानी चाहिए और जब भी न्यायालय के समक्ष पूरे तथ्य रखे जाएं, तब निर्णय लिया जाना चाहिए।
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2), हिंदू विवाह अधिनियम के समान। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (25) द्वारा परिभाषित अनुसूचित जनजातियों पर प्रथाओं की प्रयोज्यता को बाहर करता है, जब तक कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्देश न दे।
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2), हिंदू विवाह अधिनियम के समान। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (25) द्वारा परिभाषित अनुसूचित जनजातियों पर प्रथाओं की प्रयोज्यता को बाहर करता है, जब तक कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्देश न दे।
अनुच्छेद 25 के स्पष्टीकरण 11 में उन्हें हिंदू के रूप में शामिल नहीं किया गया है। छोटानागपुर काश्तकारी कला और संथाल परगना काश्तकारी (पूरक प्रावधान) अधिनियम, 1949। बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन, 1969 आदिवासियों की भूमि की रक्षा और उनकी बहाली का इरादा रखता है प्रथागत उत्तराधिकार के संचालन से, पुत्र और उसके वंशज जनजातियों द्वारा स्वयं या उसके परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा खेती के उद्देश्य से रखी गई भूमि के उत्तराधिकारी होते हैं।
धारा 76 को धारा 6 के साथ पढ़ने पर उसके अधीन प्रदान की गई प्रथा, उपयोग या प्रथागत अधिकार पर प्रभाव पड़ता है, जो अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत या आवश्यक रूप से संशोधित या समाप्त नहीं किया गया हो। कानून उस समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूद है, जो इसके द्वारा शासित है। यदि कानून को शहर की जरूरतों को पूरा करने की अपनी निर्धारित भूमिका निभानी है, तो उसे उस समाज के विचारों और विचारधाराओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए। जैसा कि पहले कहा गया है,
इसे समाज की धड़कनों और लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं के साथ समय के साथ चलना चाहिए। जैसा कि देखा गया है, बिहार के आदिवासियों में भी अब रीति-रिवाजों में उन्नति हुई है। वे बेटे और बेटी दोनों को समान रूप से पसंद करते हैं, हालांकि समान रूप से नहीं। उत्तराधिकार पितृवंशीय है धारा 14(1)
आदिवासी हिन्दू नहीं है। Adivasi Hindu Nahi केरल उच्च न्यायालय निर्णय 2012
आदेश के विरुद्ध 27 सितम्बर, 2012 को कोरमार में एड्स एसएमपी द्वारा ऑप्स में निर्णय. |
| 3 |
अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अर्थ में अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित है तथा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2(2) के अनुसार हिंदू विवाह अधिनियम अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होता है।
यदि ऐसा है, तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत पारिवारिक न्यायालय द्वारा जारी निर्देश अपीलकर्ता पर लागू नहीं होते हैं।
7. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विवाह हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था। हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न होने के पश्चात, अपीलकर्ता-पत्नी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2(2) के लाभ का दावा नहीं कर सकती है।
8. इस अपील में शामिल विवाद को समझने के लिए, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) की प्रासंगिक धारा 2(2) का संदर्भ लेना आवश्यक है। वैवाहिक अधिकार की बहाली के लिए प्रतिवादी ने ट्रायल कोर्ट में कई आधार लिए, जिन्हें अपीलकर्ता ने फैमिली कोर्ट में खारिज कर दिया,
7. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विवाह हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था। हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न होने के पश्चात, अपीलकर्ता-पत्नी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2(2) के लाभ का दावा नहीं कर सकती है।
8. इस अपील में शामिल विवाद को समझने के लिए, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) की प्रासंगिक धारा 2(2) का संदर्भ लेना आवश्यक है। वैवाहिक अधिकार की बहाली के लिए प्रतिवादी ने ट्रायल कोर्ट में कई आधार लिए, जिन्हें अपीलकर्ता ने फैमिली कोर्ट में खारिज कर दिया,
हालांकि, फैमिली कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया। लेकिन, अब पत्नी ने इस अपील में केवल एक बिंदु रखा है कि हिंदू विवाह अधिनियम अधिनियम की धारा 2(2) के तहत अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होता है। अधिनियम की धारा 2 (2) इस प्रकार है:
"2. अधिनियम का अनुप्रयोग.- (1) xxxx
- (क) xxx XXX
- (ख) XXX XXX
- (ग) xxx xxx स्पष्टीकरण.- xxx xxx
- (क) XXX XXX
- (ख) xxx xxx
- (ग) xxx xxx (2)
उप-धारा (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अधिनियम में निहित कोई भी बात संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (25) के अर्थ के भीतर किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होगी, जब तक कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्देश न दे।"
9. अधिनियम की धारा 2 (2) को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर यह पता चलता है कि अधिनियम किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होता है, जब तक कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्देश न दे।
9. अधिनियम की धारा 2 (2) को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर यह पता चलता है कि अधिनियम किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होता है, जब तक कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्देश न दे।
संविधान के अनुच्छेद 366 में अनुसूचित जनजाति शब्द की अभिव्यक्ति और अर्थ को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार, "अनुसूचित जनजातियों" का तात्पर्य ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों या ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भागों या समूहों से है, जिन्हें संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जनजाति माना जाता है, जिसे संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के साथ आगे पढ़ा जाना है।
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री संजय सैनी।
आदेश
(05.09.2013) यह धारा 482 के अंतर्गत एक आवेदन है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी-परिवादी द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंडला के न्यायालय में लंबित शिकायत प्रकरण संख्या 1969/2008, जो धारा 494 के अंतर्गत पंजीकृत है, को निरस्त किया जाए।
2. प्रतिवादी ने शिकायत प्रकरण दायर किया तथा धारा 200 के अंतर्गत उसकी गवाही तथा धारा 202 के अंतर्गत गवाहों की गवाही दर्ज करने के पश्चात आवेदक के विरुद्ध धारा 494 के अंतर्गत मामला पंजीकृत किया गया तथा उसे नोटिस जारी किया गया।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट निर्णय आदिवासी हिन्दू नहीं है | Adivasi Hindu Nahi दीपक मरावी बनाम कलाबाई 2013
आवेदक की ओर से अधिवक्ता सुश्री नीलन गोयल।अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री संजय सैनी।
आदेश
(05.09.2013) यह धारा 482 के अंतर्गत एक आवेदन है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी-परिवादी द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंडला के न्यायालय में लंबित शिकायत प्रकरण संख्या 1969/2008, जो धारा 494 के अंतर्गत पंजीकृत है, को निरस्त किया जाए।
2. प्रतिवादी ने शिकायत प्रकरण दायर किया तथा धारा 200 के अंतर्गत उसकी गवाही तथा धारा 202 के अंतर्गत गवाहों की गवाही दर्ज करने के पश्चात आवेदक के विरुद्ध धारा 494 के अंतर्गत मामला पंजीकृत किया गया तथा उसे नोटिस जारी किया गया।
 |
| 4 |
वास्तव में आवेदक के विरुद्ध धारा 494 के अंतर्गत मामला पंजीकृत किए जाने को निरस्त करने के लिए धारा 482 के अंतर्गत यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक/पति की विद्वान वकील सुश्री गोयल का तर्क है कि प्रतिवादी-शिकायतकर्ता ने स्वयं शिकायत के पैरा 1 में कहा है कि वह गोंड समुदाय से है और उसने आवेदक से वैशाख (जून माह) 1981 के महीने में गोंड समुदाय में प्रचलित रीति-रिवाज के अनुसार विवाह किया था।
3. आवेदक/पति की विद्वान वकील सुश्री गोयल का तर्क है कि प्रतिवादी-शिकायतकर्ता ने स्वयं शिकायत के पैरा 1 में कहा है कि वह गोंड समुदाय से है और उसने आवेदक से वैशाख (जून माह) 1981 के महीने में गोंड समुदाय में प्रचलित रीति-रिवाज के अनुसार विवाह किया था।
विवाह के बाद शिकायतकर्ता और वर्तमान आवेदक के विवाह से दो बच्चे भी पैदा हुए। हालाँकि, अक्टूबर 1990 के महीने में आवेदक ने अन्य सह-आरोपी व्यक्ति के आग्रह पर गोंड समुदाय में प्रचलित रीति-रिवाज के अनुसार पवित्र अग्नि के समक्ष और सप्तपदी करने के बाद वैध दूसरा विवाह किया,
इसलिए शिकायत में यह कहा गया है कि आवेदक-पति ने धारा 494 के तहत अपराध किया है और अन्य आरोपियों ने आईपीसी की धारा 494/109 के तहत अपराध किया है। कुंवर सिंह मार्को बनाम शिव दयाल सरोटे, 1998 आईएलआर के मामले में इस न्यायालय के डिवीजन बी के फैसले पर भरोसा करते हुए, उनके द्वारा यह तर्क दिया गया है
कि आदिवासी गोंड समुदाय में दूसरा विवाह स्वीकार्य है और सदस्य को एक से अधिक पत्नियां रखने की अनुमति है और उसी प्रस्ताव पर कुमारी बाई w/o आनंद राम बनाम आनंदराम नाथू ठाक (1998) 2 एमपीएलजे 584 के मामले में इस न्यायालय के सिंगल बेंच के एक अन्य फैसले पर भरोसा किया गया है जिसमें यह माना गया है
कि हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों का आदिवासी समुदाय के संबंध में कोई प्रयोज्यता नहीं है, जिसमें दूसरा विवाह अनुमेय है और यदि दूसरा विवाह संपन्न होता है तो यह विवाह शून्य नहीं होगा। डॉ सूरजमणि स्टेला कुजूर बनाम दुर्गा चरण हंसला 2001 एआईआर एससीडब्लू 711 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जोर देते हुए,
यहाँ यह प्रार्थना की गई है कि चूँकि पक्षकार आदिवासी समुदाय के सदस्य हैं और वे गोंड हैं, इसलिए आवेदक द्वारा किया गया दूसरा विवाह अमान्य नहीं है और यह एक वैध विवाह है जो उनके समुदाय में स्वीकार्य है। इसलिए आवेदक द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। इन आधारों पर, यह प्रार्थना की गई है कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत यह आवेदन स्वीकार किया जाए।
4. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सैनी ने प्रस्तुत किया कि क्या गोंड समुदाय में दूसरी शादी करने की प्रथा प्रचलित है, यह तथ्य और जांच का विषय है और इसलिए, प्रारंभिक स्तर पर प्रतिवादी-शिकायतकर्ता द्वारा दायर शिकायत मामले को खारिज नहीं किया जा सकता है।
अपने तर्क के समर्थन में, वकील ने कैलाश एस बनाम मेवालाल, 2002(11) एमपीडब्ल्यूएन 8 के मामले में इस न्यायालय के एकल पीठ के फैसले पर भरोसा रखा है। इसलिए यह प्रार्थना की गई है कि सीआरपीसी की धारा 4824 के तहत यह आवेदन स्वीकार किया जाए। खारिज किया जाए।
5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, मेरा विचार है कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत यह आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है।
6. विद्वान जेएमएफसी, मंडला के समक्ष प्रतिवादी द्वारा दायर शिकायत के अवलोकन से पता चला कि पक्ष गोंड समुदाय के हैं और इस संबंध में शिकायत के पैरा 1 को देखा गया है। इसके अलावा शिकायतकर्ता द्वारा यह भी कहा गया है
5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, मेरा विचार है कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत यह आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है।
6. विद्वान जेएमएफसी, मंडला के समक्ष प्रतिवादी द्वारा दायर शिकायत के अवलोकन से पता चला कि पक्ष गोंड समुदाय के हैं और इस संबंध में शिकायत के पैरा 1 को देखा गया है। इसके अलावा शिकायतकर्ता द्वारा यह भी कहा गया है
कि आवेदक ने आवेदक के साथ वर्ष के वैसाख महीने में वैध विवाह किया था और शिकायत के बाद के पैराग्राफ में यह दावा किया गया है कि आवेदक और शिकायतकर्ता के विवाह से दो बच्चे हुए थे। शिकायत में ऐसा कोई दावा नहीं है कि शिकायतकर्ता गु समुदाय से नहीं है।
7. अब सवाल यह है कि क्या गोंड समुदाय के रीति-रिवाजों के अनुसार दूसरी शादी जायज़ है और क्या हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान पक्षकारों पर लागू नहीं होते हैं।
7. अब सवाल यह है कि क्या गोंड समुदाय के रीति-रिवाजों के अनुसार दूसरी शादी जायज़ है और क्या हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान पक्षकारों पर लागू नहीं होते हैं।
डॉ. सूरजमणि स्टेला कुजूर (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही माना है कि यदि पक्षकार आदिवासी समुदाय के हैं तो हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान बिल्कुल भी लागू नहीं होते हैं, जिसका अर्थ यह होगा कि यदि पहली पत्नी जीवित है तो भी दूसरी शादी बिल्कुल भी प्रतिबंधित नहीं है।
कुंवर सिंह मार्को (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ ने भी यही दृष्टिकोण अपनाया था, जिसमें मुख्य न्यायाधीश श्री ए.के. माथुर (तत्कालीन माननीय न्यायाधीश) ने खंडपीठ की ओर से बोलते हुए कहा था कि आदिवासी गोंड के रीति-रिवाजों के तहत एक और पत्नी रखना जायज़ है और चूंकि गोंड समुदाय में पहली शादी के जीवनकाल में दूसरी शादी करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है,
इसलिए दूसरी शादी को अमान्य नहीं कहा जा सकता। कुमारी बाई पत्नी आनंद राम (सुप्रा) के मामले में विद्वान एकल पीठ ने भी यही दृष्टिकोण अपनाया था।
8. श्री सैनी का तर्क कि सबसे पहले प्रथा को साबित किया जाना चाहिए और उसके बाद ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि गोंड समुदाय में दूसरी शादी करना जायज़ है या नहीं, पहली नज़र में काफी आकर्षक लगता है लेकिन गहराई से जाँच करने पर मुझे लगता है
कि इसमें कोई दम नहीं है। दरअसल, शिकायतकर्ता के लिए यह ज़रूरी था कि वह शिकायत में यह दावा करे कि पहली शादी के रहते हुए या पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना गोंड समुदाय में जायज़ नहीं है। डॉ. सूरजमणि स्टेला कुजूर (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 13 में इस बिंदु को ध्यान में रखा है और स्पष्ट रूप से माना है
कि अगर शिकायत में कहीं भी यह दावा नहीं किया गया है कि कथित प्रथा में कानूनी बल है जो अभियुक्त द्वारा दूसरी शादी करने और उसके परिणामों को प्रतिबंधित करता है, तो केवल एक विवाह पर जोर देने वाली प्रथा का तर्क देना पर्याप्त नहीं है जब तक कि यह आगे तर्क न दिया जाए
कि दूसरा विवाह ऐसे पति या पत्नी के जीवित रहते हुए होने के कारण अमान्य है। उक्त निर्णय भी भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के संबंध में था। कहने की आवश्यकता नहीं है कि शिकायतकर्ता-प्रतिवादी द्वारा दायर किया गया शिकायत मामला भी भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अंतर्गत है।
चूंकि इस संबंध में संपूर्ण शिकायत में कोई भी कथन नहीं है, इसलिए मेरा मानना है कि आवेदक के विरुद्ध धारा 494 के अंतर्गत मामला दर्ज करना कानून के विरुद्ध है। इस पृष्ठभूमि में कैलाश सिंह (सुप्रा) के मामले में विद्वान एकल पीठ का निर्णय सर्वथा अलग है।
9. इसके अलावा, यदि शिकायत के पैरा 7 में किए गए कथन पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाए, तो यह पता चलेगा कि शिकायतकर्ता ने स्वयं यह दलील दी है कि प्रथा के अनुसार आवेदक-पति ने सह-आरोपियों के आग्रह पर अक्टूबर, 1990 में दूसरा विवाह किया है।
9. इसके अलावा, यदि शिकायत के पैरा 7 में किए गए कथन पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाए, तो यह पता चलेगा कि शिकायतकर्ता ने स्वयं यह दलील दी है कि प्रथा के अनुसार आवेदक-पति ने सह-आरोपियों के आग्रह पर अक्टूबर, 1990 में दूसरा विवाह किया है।
इसलिए, मेरा मानना है कि जब शिकायतकर्ता का स्वयं का मामला यह है कि उसके पति द्वारा दूसरा विवाह वैध है, तो धारा 494 के अंतर्गत अपराध दर्ज करने का प्रश्न ही नहीं उठता।
परिणामस्वरूप धारा 482 सीआरपीसी के तहत यह आवेदन स्वीकार किया जाता है और प्रतिवादी शिकायतकर्ता द्वारा दायर शिकायत मामला संख्या 1969/2008 जो धारा 494 आईपीसी के तहत पंजीकृत है और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंडला के न्यायालय में लंबित है, निरस्त किया जाता है।
परिणामस्वरूप धारा 482 सीआरपीसी के तहत यह आवेदन स्वीकार किया जाता है और प्रतिवादी शिकायतकर्ता द्वारा दायर शिकायत मामला संख्या 1969/2008 जो धारा 494 आईपीसी के तहत पंजीकृत है और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंडला के न्यायालय में लंबित है, निरस्त किया जाता है।
3POSTw.jpg)